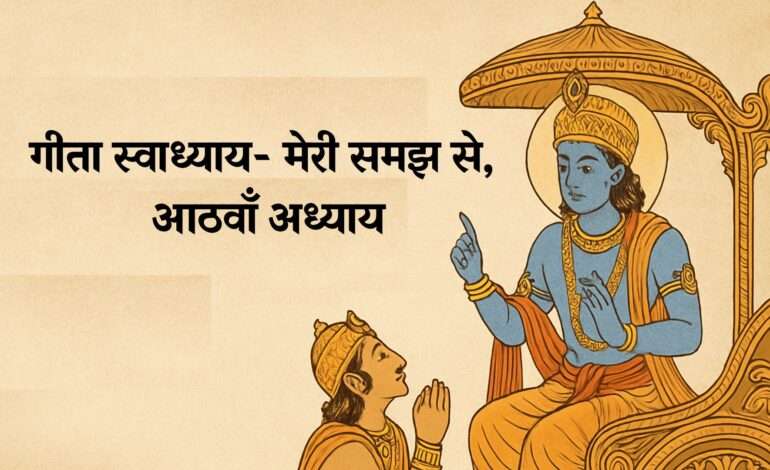
गीता स्वाध्याय- मेरी समझ से, आठवाँ अध्याय
By: Rajendra Kapil
इस अध्याय के आरम्भ में एक बार फिर अर्जुन ने भगवान कृष्ण के सामने प्रश्नों की झड़ी लगा दी. बहुत सारी बातों का समाधान मिलने के बाद भी, जिज्ञासा इतनी गहन है कि, और जानने की प्यास लगातार बढ़ती ही जा रही है. अर्जुन पूछने लगे, हे केशव, यह ब्रह्म क्या है? यह अध्यात्म क्या है? आप अधिदेव किसे मानते हैं? और यह अधियज्ञ क्या है? आप किसी योगी की स्मृति में निरंतर कैसे रहते हैं? ऐसा योगी, जो आपको सदा सिमरता है, उसकी मन:स्थिति कैसी होती है? एक भक्त, जो मृत्यु के निकट है, जिसका चित्त शरीर की बीमारियों की चिंता में घिरा है, या जो अपने परिवार की चिंता में उलझा है, वह उन सब से उबर कर, आपको अपने चित्त में कैसे बनाए रखे.
भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर तुम्हें बताता हूँ. यह जो परम ऊँ अक्षर है, इसका कभी नाश नहीं होता. जो सदा अविनाशी है, वही ब्रह्म है. यही इस संसार में “ऊँ” ओंकार ध्वनि के रूप में जाना जाता है. हर जीव के अंदर जो प्राण तत्व है, जोकि मेरा ही अंश है, वह अध्यात्म है. इसे आत्मा भी कहा जाता है. शरीर के समाप्त होने पर, यही आत्मा किसी दूसरे शरीर में चली जाती है. यही आत्मा जब घोर तपस्या के बाद मेरे धाम में आकर मेरे परम स्वरूप से मिलती है, तो ब्रह्मात्मा कहलाती है. जैसे एक नदी लंबी यात्रा के बाद, सागर में आकर अपना अस्तित्व खो कर, सागर बन जाती है, ठीक उसी तरह यह आत्मा मुझ परम् ब्रह्म में मिल, परमात्मा बन जाती है. अब सुनो, कर्म क्या क्या है? शास्त्रों द्वारा वर्णित, यज्ञ, तप, दान आदि कर्मों से मिलने वाले, सभी पुण्य फलों का त्याग, वास्तविक कर्म कहलाता है. यह कर्म जीव को ब्रह्म तक पहुँचने में सहायक होते हैं. सभी सांसारिक पदार्थ,
जो कुछ जो उत्पन्न होता है, उसका विनाश भी होता है, वह अधिभूत कहलाता है.
भगवान कृष्ण आगे समझाते हैं कि, जहाँ तक अधियज्ञ की बात है, तो हे अर्जुन, मैं ही अपने दिव्य रूप में, अधियज्ञ हूँ. जो भी भक्त मेरे इस दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए, शरीर का त्याग करता है, वह मेरे इस दिव्य स्वरूप में विलीन हो जाता है. भक्त, जो नदी के समान है, मुझ में मिल, ( मैं सागर के समान) अपार एवं विस्तृत हो, ब्रह्मात्मा बन जाती है.
यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ (६)
भावार्थ: हे कुन्तीपुत्र! मनुष्य अंत समय में जिस–जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह उसी भाव को ही प्राप्त होता है, जिस भाव का जीवन में निरन्तर स्मरण किया है।
किसी भी भक्त का अंतकाल का समय बड़ा ही नाज़ुक होता है. भक्त अंतिम समय जिस भाव को धारण कर, प्राण त्यागता है, उसे अगला जन्म उसी भाव के आधार पर मिलता है. वह नए जन्म में उसी भाव/ उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयत्न करने लगता है. प्रभु कहते हैं कि, हे कुंती पुत्र, इसलिए मैं तुम्हें यही सलाह देता हूँ कि, तू मुझे निरन्तर स्मरण करता हुआ, अपने कर्तव्य कर्म, अर्थात् युद्ध के लिए तत्पर हो जा. अगर तू वीरगति को प्राप्त हुआ, तो भी तुम मेरे धाम को ही प्राप्त होगे. प्रभु इस श्लोक में, कर्तव्य कर्म के पालन पर बहुत ज़ोर दे रहे हैं. कर्तव्य कर्म के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है. पूरी निष्ठा से किया गया हर कर्तव्य कर्म, योगी को निश्चय ही अपने परम् उद्देश्य की ओर ले जाता है. केवल एक ही शर्त है, वह सब कुछ आसक्ति रहित भाव से कर, और सब किए हुए को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दे. प्रभु को समर्पित होते ही, वह कर्तापन या कर्म के अहंकार से मुक्त हो जाता है. उसमें एक सहज शुद्धता एवं निर्मलता आ जाती है, जो प्रभु जो अत्यंत प्रिय है.
सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च ।
मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ॥ (१२)
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् ।
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥ (१३)
भावार्थ: शरीर के सभी द्वारों को वश में करके तथा मन को हृदय में स्थित करके, प्राणवायु को सिर में रोक करके योग-धारणा में स्थित हुआ जाता है।
इस प्रकार ॐकार रूपी एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करके मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मनुष्य मेरे परम-धाम को प्राप्त करता है।
इस श्लोक में प्रभु कृष्ण बताते हैं कि, मुझ तक पहुँचने का सबसे सरल उपाय है कि, भक्त अपनी सब इंद्रियों को अपने वश में करके, उनसे प्राप्त होने वाले फल के लोभ से, ऊपर उठ कर, उनसे मिलने वाले सांसारिक सुखों को त्याग कर, केवल ऊँ का उच्चारण हुआ, उसके अर्थ को पूरी गहराई से, अपने मन प्राण में बसाता हुआ, मेरे ध्यान में रमा रहे. ऐसा करने पर, मेरा भक्त निश्चय ही परम् गति यानि मेरे धाम को प्राप्त होगा. मेरा निरंतर ध्यान करने वाले योगी के लिए मैं सहज ही सुलभ हूँ. ऐसे योगी आवागमन के दुखदायी चक्र से बच जाते हैं. ऐसे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता. वह सांसारिक लोक को त्याग सीधे मेरे धाम में आ बसते हैं.
(प्रकाश-मार्ग और अन्धकार-मार्ग का निरूपण)
यत्र काले त्वनावत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः ।
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ (२३)
अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् ।
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ (२४)
धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम् ।
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥ (२५)
भावार्थ: हे भरतश्रेष्ठ! जिस समय में शरीर को त्यागकर जाने वाले योगीयों का पुनर्जन्म नही होता हैं और जिस समय में शरीर त्यागने पर पुनर्जन्म होता हैं, उस समय के बारे में बतलाता हूँ।
जिस समय ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, दिन का पूर्ण सूर्य-प्रकाश हो, शुक्ल-पक्ष का चन्द्रमा बढ़ रहा हो और जब सूर्य उत्तर-दिशा में रहता है उन छः महीनों के समय में शरीर का त्याग करने वाले ब्रह्मज्ञानी मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होते हैं।
भावार्थ : जिस समय अग्नि से धुआँ फ़ैल रहा हो, रात्रि का अन्धकार हो, कृष्ण-पक्ष का चन्द्रमा घट रहा हो और जब सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है उन छः महीनों के समय में शरीर त्यागने वाला स्वर्ग-लोकों को प्राप्त होकर अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर पुनर्जन्म को प्राप्त होता है।
प्रभु ऊपर के श्लोकों में शरीर त्यागने का सही समय बताते हैं. सूर्य देव छह माह उतरायण दिशा में होते हैं और छह महीने दक्षिणायन दिशा में चलते हैं. वैसे तो साधारण भक्त के लिए मृत्यु का समय उसके बस में नहीं होता. लेकिन सिद्ध योगी, जो निरंतर प्रभु का चिन्तन मनन करते रहते हैं, वह अपने लिए मृत्यु का उचित समय चुन सकते हैं. जैसे महाभारत की एक कथा के अनुसार, जब पितामह भीष्म युद्ध में घायल हो मृत्यु शैय्या पर पड़े थे, तो उस समय सूर्या दिशा ठीक न होने पर, वह कई दिन तक प्रतीक्षा करते रहे. कुछ दिन पीड़ा सहने के बाद, जब सूर्य दिशा उत्तरायण में आये, तो पितामह भीष्म ने प्राण त्यागे.
इसी के आधार पर प्रभु कृष्ण बताते हैं कि, मेरे पास आने के दो मार्ग हैं. एक ज्योतिर्मय मार्ग, अर्थात् शुक्ल पक्ष या सूर्य की उत्तरायण दिशा. जब कोई भक्त ऐसे शुक्ल पक्ष, या प्रकाश पक्ष में प्राण त्यागता है तो उस पक्ष के देवता उस आत्मा को मेरे लोक में ले आते हैं, और मैं उन्हें अपनी शरण में ले लेता हूँ. दूसरा मार्ग है, अंधकार मार्ग. इसे कृष्ण पक्ष या दक्षिणायन भी कहते हैं. ऐसे समय में जब कोई योगी प्राण त्यागता है, तो वह मेरे धाम तक नहीं पहुँच पाता. उन्हें इस मार्ग के, सांसारिक सुखों में लिप्त देवता, पुन: संसार के आवागमन के चक्र में धकेल देते हैं. ऐसे देवताओं का उद्देश्य यह होता है कि, इस प्राणी को अभी और तपस्या की आवश्कता है. वह भक्त को एक और अवसर देते हैं कि, भक्त प्रभु की और निष्ठा से भक्ति कर, प्रभु को पाने का पूरा प्रयास करे. प्रभु के धाम की अभिलाषा करे. उसके प्रति उसके मन मन विश्वास एवं श्रद्धा हो. और मन प्राण में एक तीव्र इच्छा हो कि वह प्रभु धाम तक पहुँचने के लिए लालायित हो उठे.
इस प्रकार इन दोनों मार्गों को जानता हुआ, कोई भी योगी मोहित नहीं होता. वह निष्काम भाव से, आसक्ति रहित भाव से, सब कर्तव्य कर्म करता रहता है. और हर किए हुए काम को, प्रभु को समर्पित करता जाता है. कामनायों का त्याग कर देता है. इंद्रियों को वश में कर, प्रभु का ध्यान करता हुआ, बस केवल एक प्रार्थना करता चलता है कि, ही प्रभु मेरा हाथ पकड़, मुझे उचित दिशा की ओर ले चलो. इस सम भाव वाला भक्त प्रभु को बड़ा प्रिय है. यह था आठवें अध्याय का ब्रह्म अक्षर ज्ञान योग. प्रभु हम सब को इस कठिन मार्ग पर चलने के क्षमता प्रदान करें.
“जय श्री कृष्ण”