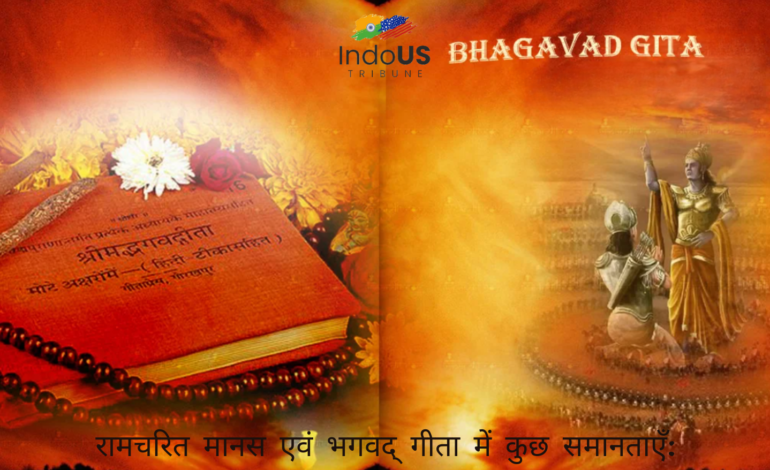
रामचरित मानस एवं भगवद् गीता में कुछ समानताएँ:
By: Rajendra Kapil
दूसरी कड़ी- दोनों रचनाओं में, भक्ति के लक्षण एवं उदाहरण
रामचरितमानस भक्ति का सागर है. उसमें भक्ति की अविरल गंगा हर कांड में बह रही है. दूसरी
ओर भगवद् गीता के बारहवें अध्याय को भक्ति योग का अध्याय माना जाता है. इस अध्याय में
भगवान कृष्ण ने अर्जुन के एक प्रश्न के उत्तर में भक्ति और भक्त के लक्षणों का विस्तृत
विवेचन किया है. अर्जुन पहले ही श्लोक में पूछता है, हे माधव,
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते |
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा: || 1||
जो अनन्य प्रेमी भक्त जन आपके सगुण रूप को भजते हैं, और जो भक्त आपके अविनाशी
सच्चिदानन्द निराकाररूप को उपासते हैं, उन दोनों में से उत्तम भक्त कौन है? इसके उत्तर में
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं:
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्न्यस्य मत्पर: |
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते || 6||
मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय |
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय: || 8||
यहाँ प्रभु स्पष्ट रूप से सगुण साकार रूप की उपासना की प्रशंसा करते हैं. भक्त के अनन्य भाव
की, उसके चिरंतन चिंतन मनन की, भक्ति को उत्तम कहते हैं. जो भक्त मुझ में अपने मन प्राण से
मुझे निरंतर भजता है. वह निश्चित रूप से मुझ में ही निवास करता है. मुझे ऐसे सगुण उपासक
बहुत प्रिय हैं. इसमें कोई संशय नहीं है.
श्री भगवद् गीता में अगर लक्षण हैं, तो राम चरित मानस में उन्हीं लक्षणों को उजागर करने वाले
चरित्र हैं. भक्तों में सर्वोपरि हनुमान जी एवं विभीषण जी का नाम सामने आता है. इन दोनों
भक्तों का अस्तित्व ही राम नाम से आरंभ होता है, और पूर्ण जीवन राम काज को समर्पित हुआ
दिखाई पड़ता है. हनुमान जी पहले पहल जब, किष्किन्धा कांड में, अपने स्वामी रामजी को
मिलते हैं, तो तुरंत पहचान लेते हैं. और पहचानते ही, उसी क्षण, उनके चरणों में गिर, लोटपोट हो
जाते हैं:
ता पर मैं रघुबीर दोहाई, जानऊँ नहि कछु भजन उपाई
अस कहि परेउ चरन अकुलाई, निज तनु प्रगटी प्रीति उर लाई
हनुमान जी को चरणों में पड़ा देख, रामजी ने अपने प्रिय भक्त को उठा कर हृदय से लगा लिया.
और कहने लगे, सब मुझे समदर्शी कहते हैं, लेकिन मेरे लिये भक्त से बढ़ कर कोई नहीं:
समदरसी मोहि कह सब कोऊ, सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ
सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमंत
मैं सेवक सचराचर रूप, स्वामी भगवंत
रामजी तो भक्त हनुमान से इतने प्रभावित होते हैं, कि उसे अपने साथ चल रहे लक्ष्मण भाई से
भी अधिक मान देने पर बाध्य हो उठते हैं:
सुनु कपि ज़िय मानसि जनि ऊना, तै मम प्रिय लछिमन ते दूना
तुलसी बाबा ने हनुमान चालीसा में भी हनुमान जी के बारे यहाँ तक लिख डाला:
रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई
अर्थात् रामजी हनुमान जैसे भक्त को सदा, अपने भाइयों से भी ऊपर कर, मानते रहते हैं.
गीता में उसी बारहवें अध्याय में आगे चल कर, भगवान कृष्ण ने भक्ति के लक्षणों को और भी
खुल कर परिभाषित किया.
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र: करुण एव च |
निर्ममो निरहङ्कार: समदु:खसुख: क्षमी || 13||
सन्तुष्ट: सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय: |
मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्त: स मे प्रिय: || 14||
भक्त वोह है, जो अन्य प्राणियों से द्वेष नहीं करता. हमेशा स्वार्थ रहित है. सबसे प्रेम करने
वाला है. ममता और आसक्ति से कोसों दूर है. भक्त का एक सबसे बड़ा लक्षण यह है, कि वोह
अहंकार रहित है. क्षमाशील है. वह रामकाज के लिए सदा तत्पर एवं दृढ़ निश्चयी है. हमेशा
संतुष्ट रहते हुए, अपने मन और बुद्धि को प्रभु चरणों में लगाये रहता है.
अब इसी तुला पर हनुमान जी के चरित्र को तोलिये. वह किसी से द्वेष नहीं करते. सबको प्रेम
और उत्साह से मिलते हैं. राम काज के लिए सदा तत्पर रहते हैं. दुख और सुख में सम भाव
बनाये रखते हैं. लँका में जब मेघनाद उन्हें ब्रहास्त्र में बाँध लेता है, तो भी वोह हँसी ख़ुशी उसके
साथ रावण सभा पहुँच कर, सबसे हँसी ठठौली करते रहते हैं. रावण से प्रश्नोत्तर के बाद, जब
रावण उनकी पूँछ में आग लगा कर जलाने का दण्ड सुनाता है, तो उस सजा को सहज स्वीकार
कर तथा “जय श्री राम” का उदघोष कर पूरी लँका को तहस नहस कर देते हैं. इस सबके बावजूद
इतने विनम्र एवं अहंकार रहित हैं, कि लँका से लौट कर, जब रामजी के सामने प्रस्तुत होते हैं, तो
राम जी पूछते हैं, अरे हनुमान:
कहु कपि रावन पालित लंका, केहि बिधि दहेऊ दुर्ग अति बंकातुमने लँका कैसे जलायी? हनुमान जी बड़े विनम्र भाव से कहते है:
साखा मृग कै बड़ी मनुसाई, साखा ते साखा पर जाई
नाघि सिंधु हाटक पुर जारा, निसीचर गन बधि बिपिन उजारा
सो सब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरि प्रभुताई
हे स्वामी, मैं तो मात्र एक बंदर हूँ, मुझे तो वृक्षों पर केवल कूदना आता है. लँका में जो कुछ भी
हुआ, वह सब आपकी कृपा का प्रताप था, उसमें मेरा योगदान कुछ भी नहीं था. यह है भक्त का
अहंकार रहित, स्वामी के प्रति पूर्ण समर्पण भाव. ऐसी सरल हृदयी भक्ति को देख प्रभु गदगद
हो गए, और सबको बताने लगे:
निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा.
गीता में एक दो और सुंदर श्लोक है. इसमें यह वर्णित है, कि भक्त का व्यवहार कैसा होता है. वह
सुख में हर्षित नहीं होता.वह दुख में विचलित नहीं होता. प्रशंसा पाकर फूलता नहीं है, और निंदा
सुन कर क्रोधित नहीं होता. भक्त शुभाशुभ संपूर्ण कर्मों का परित्यागी होता है. ऐसी भक्ति से
युक्त भक्त मुझे बहुत प्रिय है. इस तरह का भक्त, शत्रु और मित्र में, मान और अपमान में, सर्दी
और गर्मी में, तथा सुख और दुख जैसे द्वन्दों में, हमेशा आसक्ति रहित रहता है.
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ् क्षति |
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्य: स मे प्रिय: || 17||
सम: शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो: |
शीतोष्णसुखदु:खेषु सम: सङ्गविवर्जित: || 18||
तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् |
अनिकेत: स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नर: || 19||
अब रामजी के व्यक्तित्व की एक छवि देखिए:
अयोध्या काण्ड में रामजी के विवाह के बाद, महाराज दशरथ उन्हें गद्दी पर बैठाने के तैयार हो
जाते हैं. मंत्रियों से सलाह कर, उन्हें युवराज घोषित कर, उनके राज्य तिलक की घोषणा कर देते
हैं. सारी अयोध्या इस ख़ुशी के समाचार से अति प्रसन्न है. परंतु उसी समय नियति अपना खेल,
खेल जाती है. मंथरा और कैकेयी की मिली भगत से सारा पासा पलट जाता है. राम को राज्य
तिलक की बजाय एक संन्यासी वेश में वनवास के लिए निकलना पड़ता है. लेकिन परिस्थिति
परिवर्तन के बाद भी रामजी के मुख पर शिकन तक नहीं आती, तुलसी बाबा इस संदर्भ में लिखते
हैं. रामजी का मुखारविंद न तो राज्याभिषेक की बात सुन कर प्रसन्न हुआ, और न ही वनवास की बात सुन कर मलिन हुआ. ऐसी सदा शांत रहने वाली रामजी के मुख कमल की छवि, मेरे लिए सदा मंगलमय हो.
मानस में एक और परम भक्त का उल्लेख है, जिसका नाम है, विभीषण. रावण उसे हर समय
इसलिए नीचा दिखाता रहता है, कि वोह भक्त प्रकृति का सीधा साधा राक्षस है. जिसमें राक्षसों
वाले कोई तामसिक गुण नहीं हैं. वह भी एक भक्त के लक्षणों के अनुसार निंदा और स्तुति दोनों
ही अवस्थाओं में सम भाव से अपना जीवन यापन करता है. रामजी की सेना जब लँका के द्वार
जा पहुँचती है, तो रावण अपने मंत्रियों से सलाह करता है. सभी मंत्री रावण की चापलूसी कर, उसे
मीठी मीठी सलाह देते हैं. ऐसे में विभीषण रावण को सीता लौटाने की, भिन्न सलाह देता है.
सुनहु नाथ सीता बिन दीन्हे, हित न तुम्हार सम्भु अज कीन्हे
लेकिन रावण को उसकी सलाह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और वोह क्रोधित हो उठता है.
विभीषण को भरी सभा में लात मार, दुत्कार देता है. फिर भी विभीषण अपने, भले भक्त
स्वभाव, के चलते यही कहता है, कि आप मेरे पिता समान हैं, आपने मुझे पर चरण प्रहार किया,
कोई बात नहीं. फिर भी आपका हित रामजी की शरण में जाने से ही होगा, और कोई दूसरा
उपाय नहीं है:
रामु सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरि
मैं रघुबीर सरन अब, जाऊँ देहु जनि खोरी
इस सब विवेचन से स्पष्ट हो जाता है, की अगर भगवद् गीता में भक्ति के लक्षणों का उल्लेख
है तो, रामचरित मानस में भक्ति को साक्षात चरितार्थ करने वाले पात्र हैं. हनुमान जैसे चरित्र,
जिन्होंने भक्ति को, अपने दैनिक जीवन में उतार, भक्ति की पराकाष्ठा के ज्वलंत उदाहरण, हम
सब के लिए बनाये. रामचरित मानस और भगवद् गीता में प्रतिपादित यह भक्ति भाव विश्व भर
में फैले, हिंदू समाज की, श्रद्धा और विश्वास के सुदृढ़ आधार स्तम्भ हैं. मेरा इस भक्तिभाव एवं
भक्ति से ओत प्रोत भक्तों को सादर नमन!!!