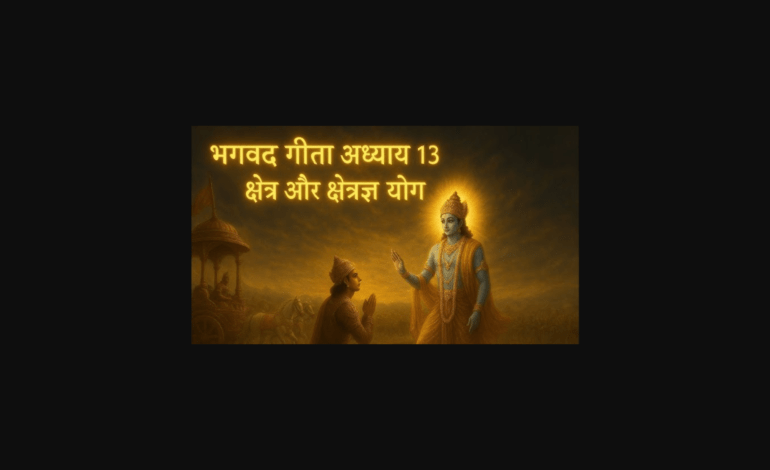
गीता स्वाध्याय, मेरी समझ से – तेरहवाँ अध्याय
By: Rajendra Kapil
यह अध्याय अद्भुत है. इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को वोह ज्ञान दे रहे हैं, जोकि सामने दीख रहा है, अर्थात् शरीर. साथ ही उसके बारे में, जो नहीं दीख रहा है, अर्थात् आत्मा. यह सर्वविदित है कि, आत्मा इस शरीर को चलायमान रखती है, इसका प्राण है. इस अध्याय का विषय है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ योग. क्षेत्र यह शरीर है और क्षेत्रज्ञ आत्मा है. क्षेत्र स्थूल है, जबकि क्षेत्रज्ञ सूक्ष्म है. इसको सरल भाषा में समझने की दृष्टि से एक उदाहरण का सहारा लेते हैं, जहां दोनों ही तत्व स्थूल हैं. क्षेत्र एक खेत की तरह है जबकि क्षेत्रज्ञ एक किसान के रूप में है. किसान खेत में कुछ भी बो सकता है. खेत किसान की कर्म भूमि है. वह अगर उसमें आम बोयेगा तो आम ही पायेगा. लेकिन अगर वह उसमें बबूल बोयेगा, तो बबूल के काँटे ही पायेगा. खेत पर वातावरण (परिवेश) का भी असर होगा. इसी तरह हम अपने शरीर में जिस प्रकार के संस्कार डालेंगे, हमारे कर्म भी, उसी प्रकार से फलीभूत होंगे. अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा. हमारा क्षेत्रज्ञ, हमारा मन, उन कर्मों को उचित दिशा दिखाने में सहायक होता है.
हमारा यह शरीर, जो हमारे माता पिता की देन है, उसमें स्थित आत्मा प्रभु का अंश है. शरीर की अपनी सीमाएँ हैं. शरीर में अनेक प्रकार के विकार हैं. शरीर में दस ज्ञान इंद्रियाँ हैं, पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं. मन बुद्धि है, अहंकार है, धैर्य है. और यह सब हमें जगत के विभिन्न कर्मों को करने में सहायक होते हैं. यह हमें अच्छी दिशा में भी ले जा सकते हैं और ग़लत दिशा में भी भटका सकते हैं. यह दिशा निर्देश करने वाला होता है, हमारा मन या बुद्धि. यही बुद्धि तत्व है, क्षेत्रज्ञ. वह हमारे शरीर का जाननहार हैं. वह शरीर की हर अच्छी बुरी शक्ति को पहचानता है. इसीलिए उसे अच्छी या बुरी दिशा प्रदान कर सकने में सक्षम हैं.
अब आगे भगवान कृष्ण बताते हैं कि, कैसे एक जागरूक योगी या क्षेत्रज्ञ किस प्रकार दोषों से बचता हुआ, अपनी इंद्रियों को साधता हुआ, धैर्य और संयम से, अपने पूज्य गुरुओं के आशीर्वाद से, मुझ तक पहुँच सकता है. नीचे के श्लोकों में, प्रभु ने बताया है कि, योगी को किन किन भावों को, अपनाना चाहिए और किन किन भावों से बचना चाहिए?
अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् ।
आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः ॥ (८)
इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च ।
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥ (९)
असक्तिरनभिष्वङ्ग: पुत्रदारगृहादिषु ।
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ (१०)
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ।
विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥ (११)
अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्वज्ञानार्थदर्शनम् ।
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ (१२)
भावार्थ : विनम्रता (मान-अपमान के भाव का न होना), दम्भहीनता (कर्तापन के भाव का न होना), अहिंसा (किसी को भी कष्ट नहीं पहुँचाने का भाव), क्षमाशीलता (सभी अपराधों के लिये क्षमा करने का भाव), सरलता (सत्य को न छिपाने का भाव), पवित्रता (मन और शरीर से शुद्ध रहने का भाव), गुरु-भक्ति (श्रद्धा सहित गुरु की सेवा करने का भाव), दृड़ता (संकल्प में स्थिर रहने का भाव) और आत्म-संयम (इन्द्रियों को वश में रखने का भाव)
इन्द्रिय-विषयों (शब्द, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श) के प्रति वैराग्य का भाव, मिथ्या अहंकार (शरीर को स्वरूप समझना) न करने का भाव, जन्म, मृत्यु, बुढा़पा, रोग, दुःख और अपनी बुराईयों का बार-बार चिन्तन करने का भाव।
पुत्र, स्त्री, घर और अन्य भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त न होने का भाव, शुभ और अशुभ की प्राप्ति पर भी निरन्तर एक समान रहने का भाव।
मेरे अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को प्राप्त न करने का भाव, बिना विचलित हुए मेरी भक्ति में स्थिर रहने का भाव, शुद्ध एकान्त स्थान में रहने का भाव और सांसारिक भोगों में लिप्त मनुष्यों के प्रति आसक्ति के भाव का न होना।
निरन्तर आत्म-स्वरूप में स्थित रहने का भाव और तत्व-स्वरूप परमात्मा से साक्षात्कार करने का भाव यह सब तो मेरे द्वारा ज्ञान कहा गया है और इनके अतिरिक्त जो भी है वह अज्ञान है।
प्रभु ने बहुत कुछ हमारे हाथ में दिया है. कर्म करने का अधिकार. पूरी निष्ठा और मेहनत का अधिकार. लेकिन यह मेहनत हमें कहाँ ले जाएगी? उसकी बागडोर उन्होंने अपने हाथ में रखी है. इसलिए उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जो अनादि है, जो अविनाशी है, जो परम ब्रह्म है, जो इस इस जीवन का परम उद्देश्य है, वह सब मेरे आधीन है. मैं ही निश्चित करता हूँ कि, किसकी यात्रा कितनी शुद्ध है. मुझे पता रहता है किं, किसकी यात्रा कितनी निश्छल है, और उसी के अनुसार मैं उस योगी को उचित फल देता हूँ.
सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।
असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च ॥ (१५)
भावार्थ: वह परमात्मा समस्त इन्द्रियों का मूल स्रोत है, फिर भी वह सभी इन्द्रियों से परे स्थित रहता है वह सभी का पालन–कर्ता होते हुए भी अनासक्त भाव में स्थित रहता है और वही प्रकृति के गुणों (सत, रज, तम) से परे स्थित होकर भी समस्त गुणों का भोक्ता है।
यहाँ प्रभु एक बड़ी रहस्यमयी बात बताते हैं कि, हे अर्जुन, जिस शारीरिक विकारों और विषयों में लोग फँसें हुए हैं, मैं उन्हें भली भाँति जानता हूँ. क्योंकि वोह सब मेरे द्वारा बनाए हुए हैं. मैं उन सबमें विराजमान होते हुए भी, उन सबसे निर्लिप्त हूँ. मैं विषयों की आसक्ति से पूर्णतया परिचित हूँ, वह एक साधारण योगी को आसानी से बाँध लेती है. लेकिन एक सच्चा योगी, उसकी इस कमज़ोरी को जान, उनमें उलझता नहीं है.
उससे तटस्थ रह कर, उन्हें भोगता है, परन्तु उसमें लिप्त नहीं होता.
मैंने तुम्हें यह ज्ञान, तुम्हारे अंदर छिपे हुए क्षेत्रज्ञ को भी, दे रखा है कि, मेरी यह प्रकृति और माया बाँधने वाली है. इससे सावधान रहो. संसार में रह कर इसे भोगों, इसकी कमज़ोरी को पहचानो, और इसे अपने परम उद्देश्य, प्रभु प्राप्ति के लक्ष्य में, बाधा मत बनने दो.
कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ।
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ (२१)
भावार्थ: जिसके द्वारा कार्य उत्पन्न किये जाते है और जिसके द्वारा कार्य सम्पन्न किये जाते है उसे ही भौतिक प्रकृति कहा जाता है, और जीव (प्राणी) सुख तथा दुःख के भोग का कारण कहा जाता है।
इस संसार में रह कर एक योगी, प्रकृति से उत्पन्न, त्रिगुणात्मक (सत्व, राजस और तामस) पदार्थों को भोगता है, और उनके परिणाम स्वरूप, अच्छी और बुरी योनियों में, जन्म लेता है. लेकिन देह में स्थित आत्मा, सूक्ष्म रूप से उन सब कर्मों की साक्षी बन जाती है. यही हमें अच्छे और बुरे की समझ प्रदान करती है. हमें उचित दिशा दिखाती है. वही हमारे भीतर, बुराई को समाप्त करने वाला महादेव बन जाती है. वही अच्छाई को सृजन करने वाली ब्रह्मा की शक्ति बन जाती है. जो योगी इस तत्व ज्ञान को जान लेता है, वह जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठ, मेरे धाम को प्राप्त होता है.
यावत्सञ्जायते किञ्चित्सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् ।
क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्धि भरतर्षभ ॥ (२७)
भावार्थ: हे अर्जुन! इस संसार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है और जो भी चर–अचर प्राणी अस्तित्व में है, उन सबको तू क्षेत्र (जड़ प्रकृति) और क्षेत्रज्ञ (चेतन प्रकृति) के संयोग से ही उत्पन्न हुआ समझ।
जो योगी नष्ट होते हुए इस चराचर जगत को, जहाँ सब कुछ नाशवान है. उसमें रह कर, मुझ सदा अविनाशी ब्रह्म के, सिमरन में लगा रहता है, जो सभी प्राणियों को समभाव से, बिना किसी मोह और आसक्ति के, प्रेम से व्यवहार करता है, वह योगी मुझे अत्यंत प्रिय है. वह इस प्रकृति के कण कण में मेरे दर्शन करता है. हर वस्तु में, मुझे साक्षात देखता है.
यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति ।
तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ (३१)
अनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्मायमव्ययः ।
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ (३२)
भावार्थ: जब जो मनुष्य सभी प्राणीयों के अलग–अलग भावों में एक परमात्मा को ही स्थित देखता है और उस एक परमात्मा से ही समस्त प्राणीयों का विस्तार देखता है, तब वह परमात्मा को ही प्राप्त होता है। हे कुन्तीपुत्र! यह अविनाशी आत्मा आदि–रहित और प्रकृति के गुणों से परे होने के कारण शरीर में स्थित होते हुए भी न तो कुछ करता है और न ही कर्म उससे लिप्त होते हैं।
इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जो योगी जन, जान जाते हैं, वह संसार के सभी विषयों और विकारों से घिरे होने के बावज़ूद, प्रभु में निरन्तर समर्पित रहते हैं. वह परमात्मा के परम तत्व को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेते हैं. यह ज्ञान देखने पढ़ने में सरल है, लेकिन है, अति गूढ़. इसकी गहनता को समझने के लिए, प्रभु कृपा की बहुत आवश्यकता है. जो सच्चे हृदय से प्रयत्न करते हैं, उन्हें यह कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होती है. “जय श्री कृष्णा”